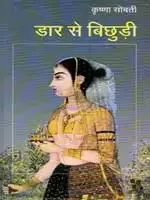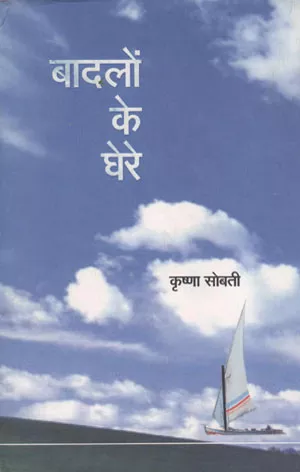|
कहानी संग्रह >> डार से बिछुड़ी डार से बिछुड़ीकृष्णा सोबती
|
120 पाठक हैं |
||||||
इसमें नारी मन की करुण-कोमल भावनाओं, आशा-आकांक्षाओं और उसके ह्रदय को मथते आवेग-आलोड़न का ममस्पर्शी स्वरूप का वर्णन किया है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
पाशो अभी किशोरी ही थी, जब उसकी माँ विधवा होकर शेखों की हवेली जा चढ़ी।
ऐसे में माँ ही उसके मामुओं के लिए कुलबोरनी नहीं हो गई, वह भी
सन्देहास्पद हो उठी। नानी ने भी एक दिन कहा ही
था-‘‘सँभलकर री, एक बार का थिरका पाँव ज़िन्दगानी धूल में मिला देगा!’’
लेकिन थिरकने-जैसा जो पाशो की ज़िन्दगी में कुछ था ही नहीं, सिवा इसके कि वह माँ की एक झलक देखने को छटपटाती और इसी के चलते शेखों की हवेलियों की ओर निकल जाती। यही जुर्म था उसका। माँ ही जब विधर्मी बैरियों के घर जा बैठी तो बेटी का क्या भरोसा। जहर दे देना चाहिए कुलच्छिनी को, या फिर दरिया में डुबो देना चाहिए !... ऐसे ही खतरे को भाँपकर एक रात माँ के आँचल में जा छुपी पाशो, लेकिन शीघ्र ही उसका यह शारण्य भी छूट गया, और फिर तो अपनी डार से बिछुड़ी एक लड़की के लिए ठौर-ठिकाना त्रासद ही बना रहा।
लेकिन थिरकने-जैसा जो पाशो की ज़िन्दगी में कुछ था ही नहीं, सिवा इसके कि वह माँ की एक झलक देखने को छटपटाती और इसी के चलते शेखों की हवेलियों की ओर निकल जाती। यही जुर्म था उसका। माँ ही जब विधर्मी बैरियों के घर जा बैठी तो बेटी का क्या भरोसा। जहर दे देना चाहिए कुलच्छिनी को, या फिर दरिया में डुबो देना चाहिए !... ऐसे ही खतरे को भाँपकर एक रात माँ के आँचल में जा छुपी पाशो, लेकिन शीघ्र ही उसका यह शारण्य भी छूट गया, और फिर तो अपनी डार से बिछुड़ी एक लड़की के लिए ठौर-ठिकाना त्रासद ही बना रहा।
डार से बिछुड़ी
एक नौसिखिए लेखक की रचनात्मक क्षमताओं और सीमाओं से अलग ‘डार से
बिछुड़ी’ के सीधे सरल पाठक की संरचना में उसकी मूल सम्भावनाएँ
पहले
से ही निहित थीं। पुराने वक्तों के आख्यान ने स्वयं अपना कथ्य कुछ ऐसे
संयम से निर्धारित किया कि पहले वाक्यांश ने ही लेखक को चौंका दिया।
जिएँ ! जागें ! सब जिएँ-जागें !
अच्छे बुरे, पराए-अपने जो भी मेरे कुछ लगते थे—सब जिएँ !
‘डार से बिछुड़ी’ का सहज सीधा पाठ बिना किसी शिल्प के सहारे स्वयं ही अपने समय सूत्र गूँथता गया और मेरे बाहर के कथ्य को कहानी की आन्तरिकता की ओर मोड़ ले गया। मुझे इस दबाव का अहसास तक न हुआ। इतना ही लगा कि मैं मात्र इसे प्रस्तुत करने के निमित्त हूँ।
‘डार से बिछुड़ी’ का पाठ लिखने में कुछ ऐसा बना कि जैसे पहले ही लिखी जा चुकी इबारत को मन से कागज पर उतारना हो। कोई झिझक, सन्देह या भाषायी उलझन नहीं हुई और फिरंगी की छावनी में पहुँच कहानी अपने आप ही समाप्त हो गई।
लिफाफे पर ‘निकष’—इलाहाबाद का पता लिखा और ‘डार से बिछुड़ी’ को डाक से ‘निकष’ के सम्पादक धर्मवीर भारती को विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया। मन में न छपने की बेचैनी थी और न ही उत्सुकता। नए लेखक वाली कोई चिन्ता और उत्तेजना भी नहीं थी।
‘निकष’ ने जब इसे विशेष कृति करके प्रकाशित किया तो देखकर विस्मय हुआ और न ही विशेष उल्लास की प्रतिक्रिया। ‘डार से बिछुड़ी’ के पाठ से जो उम्मीद उसके लेखक को थी, ‘निकष’ सम्पादक ने उसकी ताईद की थी। इतना कम नहीं था।
‘निकष’ में कहानी को पढ़ा। कहीं कुछ बदला न गया था। कोई परिवर्तन नहीं। सही समय पर मैं आश्वस्त हुई। ‘डार से बिछुड़ी’ के प्रकाशन के साथ ही मेरी रचनाओं पर नजर रखी जाने लगी। लेखक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार और भला क्या हो सकता था ! ‘डार से बिछुड़ी’ के पाठक और सुधी आलोचकों, पाठकों के प्रति गहरे भाव से कृतज्ञ हूँ। हाल ही में जब इसे पढ़ा तो लगा कहानी कहने की यह रफ्तार मुझे अब भी कायम रखनी चाहिए थी। विनम्रतापूर्वक इतना ही कि अपने बलबूते पर मेरे हाथ से उधड़ती चली गई।
विभाजन के बाद के दिन थे। दिल्ली के आकाश पर उतरा हुआ था फरवरी का पत्तों और हवाओं भरा उड़ता-फड़फड़ाता मौसम। अपने जन्म के महीने में मैं हमेशा कुछ अस्थिर सी हो उठती हूँ। धूल-भरी हवाओं सी हरहराती हूँ। बैसाख के उतरने से पहले उखड़-सी जाती हूँ। बहती सरसराती हवाएँ जाने मुझसे क्या कहती हैं। अन्तर की रहस्य-पट्टी से जाने कैसे-कैसे उदास फीके सन्देश भेजती हैं, जैसे कहीं भगदड़ मची हो। दीवारें हिल रही हैं। दरारें दीख रही हों।
फिर वही दिल दहलाता शोर—
अल्लाह ओ अकबर।
हर-हर महादेव।
विभाजन
बँटवारा।
1947।
सुबह-शाम नई दिल्ली की टैंकर से धुलनेवाली तारकोली सड़कों की रंगत बदल गई थी। पटरियाँ उदास, गुस्सील, गमगीन शरणार्थियों को टोलियों से अटी पड़ी थीं। मैली-कुचैली, पगड़ियाँ और दुपट्टे। घायल लुटे नुचे लोगों के ठट्ट के ठट्ट। कैम्प।
बेवतनों के नए नागरिक वार्ड बन रहे हैं।
अपने ठीयों से उखड़े हुए, जड़ों से दूर बदहवास, फिक्रमन्द ख़लकतें और एक दूसरे को रौंदता भाषायी शोर ! खड़े-खड़े लड़ाई-झगड़े। अपनी तल्खियों को उतार फेंकने के लिए तू-तू मैं-मैं, हाथापाई, धक्का-मुक्की। जाने किस-किस शहर के मुर्दा साये बचे-खुचे अपने इलाकेवालों के साथ भटकते छितरते-छिटकते राजधानी में आ जुटे थे।
भीड़ कभी पी ब्लाक, कभी री-हैबिलिटेशन मंत्रालय, कभी पुराना किला, फिरोजशाह कोटला, किंग्सवे कैम्प। कभी रोटी-मजूरी की जुगाड़ में तुर्कमान अजमेरी गेट, काज़ी हौज, खारी बाउली, फतेहपुरी, लाल किला, जामा मस्जिद। चाँदनी चौक।
एक दुपहर मैसोनिक लॉज की डिस्पैंसरी पर लगी लाइनों पर खड़े शरणार्थियों के कार्ड बनवाने की ड्यूटी लगी थी हमारे ग्रुप की। वहीं खड़ी भीड़ में माँ के कंधे से लगे एक बच्चे का भयानक चेहरा देखकर दिल दहल गया। एक आँख और माथे पर लगे दो गहरे घाव। ऊपर भिनभिनाती मक्खियाँ।
विभाजन जब होना ही था तो यह वहशीपन क्यों न रोका जा सका ! नस्लकुशी ?
अपने को घुड़का। बस। इस ओर सिर्फ देखो, उस पर सोचो नहीं।
सिंधिया हाउस का चौराहा क्रास कर कर्जन रोड की पटरी चलने लगी थी। घर लौटते हुए चाल में गहरी बेहिम्मती, थकान। अंग्रेजी हुकूमत का यहाँ से अलग होने का क्या और कोई रास्ता नहीं था !
चलते-चलते आसमान की ओर देखा। लगा एक बहुत बड़ी रस्सी पर ज़ख्मी घायल और मरे हुए लोगों के कपड़े एक साथ सूख रहे हैं। घबराकर अपने को धमकाया। खबरदार। अब इन ख्यालों से अपने को दूर रखो। परे झटक दो और सड़क के साथ-साथ लगे इन छाँहदार हरे भरे पेड़ों की ओर देखो। अपनी हस्ती में मजबूती से जमे हैं और अपनी गहरी जड़ों से। जो उखड़कर सड़कों पर पड़े हैं—उनके लिए जो भी कर सको करो।
पास से गुजरी साइकिल की आवाज़ से चौकी।
यह क्या ?
कर्ज़न रोड की पटरी पर आखों के सामने शाहआलमी प्रकट हो गया। सजी-बनी छोटी-बड़ी दुकानें-चुस्त-चालाक-जवान-बूढ़ी अधेड़ भीड़। माँओं की उँगलियों पकड़े बच्चे। हिन्दुआनियाँ, मुसलमानियाँ, रंग-बिरंगी चुन्नियाँ, चुटले, चूड़ियाँ, सब्जियाँ, फल ललारियों के यहाँ सूखती पगड़ियाँ। एकाएक कोई मुखड़ा झिलमिलाया जैसे भीड़ में से कोई शिलालेख ऊपर आया।
नकोर कंवर का शरमाता, इतराता मुखड़ा। पीले छींट के जोड़े पर हरी-भरी ओढ़नी। चुन्नी के छोर को मुँह में दबाए आँखों से हँसती यह लड़की कहाँ से आ रही है। आँखों से हँसती सयानी होने को मचलती यह बचपनी लड़की। शायद कंजक पुजाने का होगा यही इसका अन्तिम अवसर। फिर बँध जाएगी यह अमावस्या और पूर्णिमा की परिक्रमा से। रजस्वला। मुनिया गुणिया बन जाएगी।
इस लड़की का भला नाम क्या होगा।
पूँछूँ।
भीड़ में अदृश्य हो गई वह लड़की। और मैं चलने लगी सर्राफे की ओर। रुपहली सुनहली जेवर और झक्क मोतियों की जड़त।
मोड़ से बाएँ मुड़ती हूँ।
सोबतियों की हवेली।
हवेली का ऊँचा, चौड़ा पीतल की कीलोंवाला लड़की का पुराना दरवाजा।
फाटक की चौड़ाई और ऊँचाई बाँटते अलग-अलग चार शहतीर। एक-एक के दो-दो टुकड़े। पहले एक को ऊपर उठाओ, फिर दूसरा। इधर का। उधर का। उस पर लटक रहा है ककराली का लोहारी जन्द्रा। इसकी ताली अब किसके पास होगी। जो इधर से वहाँ पहुँचे हैं उनके पास कि उधर वालों के हाथ।
इधर।
उधर।
सामने बड़े सहन के बीच ऊँचे चबूतरे पर पानी की कुँई। लोहे की चरखड़ी। गदर, लड़ाई और भगदड़ों में पानी तो हो पीने वालों के लिए। अन्दर जाते लम्बे बड़े गलियारे पर मुखद्वार। छोटी ईंट की बड़ी ड्यौढ़ी। ड्यौढ़ी के दोनों ओर से ऊपर की मंजिल की ओर जाती सीढ़ियाँ। नीचे किनारे से मुड़ती तहखानों की ओर उतरती सँकरी पैड़ियाँ। मैं जितनी बार वहाँ जाती उतनी बार कई-कई बार नीचे जाती पैड़ियाँ उतरती और दूसरे घुमाव पर रुकती और वापस लौट आती। एक दिन ऊपर से देख रही माँ ने आवाज़ दी—क्या कर रही हो वहाँ। यह खेलने की जगह नहीं।
मैं तहखाने की ओर जा रही थी।
फिर रुक क्यों गई !
डर लगता है। वहाँ साँप है।
तो लौट आओ।
इसे कैसे देख सकती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ। कैसे देखूँ।
ऐसा कोई बन्दा नहीं जो तहखाने में जाए बिना उसे देख सके। इसका ख्याल छोड़ दो।
इसके जवाब के लिए मुझे क्यों रुकना था। जल्दी-जल्दी सीढ़ियाँ उतर गई और तहखाने का पल्ला धकियाया और किवाड़ का आधा पाट चरमराया। और इस आधे का टुकड़ा खिसियाना सा खुला। तहखाने की बासी-मुसी सीलन-भरी दुर्गन्ध नाक में घुस गई। पहले अपने कपड़ों को झाड़ा। आँखें गड़ाईं। अन्दर अँधेरा है। वहाँ से उभरी छोटी सी लीक रोशनी की। सामने की दीवार पर झरोखी है। देख लूँगी। कुछ को देख सकूँगी। कुछ-कुछ दिखता है। वह क्या ? टँगने पर लटक रहे हैं, लिहाफ़। चिमगादड़। और यह क्या ? दो बटनों की-सी आँखोंवाला उल्लू। उल्लू ही है। चुपचाप बैठा है। चिमगादड़ तो फड़फड़ाता है। बालों में फँस जाता है। यह बड़े-बड़े मटके। इनमें सिक्के होंगे।
सिक्के और तलवारें—लड़ाई के वक्त छावनी और शहर में अंग्रेजों का पहरा लग गया था। तहखानों और सिक्ख-फिरंगी युद्ध की जाने कितनी कहानियाँ हमने सुन रखी थीं।
गुजरात के चिल्लियाँवाले मैदान में तीसरी लड़ाई में अंग्रेजों ने हमें हराकर पंजाब को जीता था।
अपनी सेनाओं को पराजित कर अंग्रेजों ने शहर-भर में अपनी विजय का ऐलान कर दिया था। गलियों, नाकों और हवेलियों के मुख्य द्वारों पर फिरंगी गारद के पहले लग गए। रात के पहले पहर हमारे परिवार की सयानी पुरखन तहखानों में उतरी। अँधेरे में हरिसिंगे सिक्के झोली में डाले और पैड़ियों से ऊपर चढ़ी। जाने किस हड़बड़ाहट में सिक्के नीचे गिर पड़े और ड्योढ़ी के सामने बिखर गए। गारद ने मुड़कर देखा तो सयानी पुरखन ने रोबीली आवाज़ में हुक्म दिया—उठाओ और इधर लाओ। मुझे दो।
आवाज़ थी कड़ाकेदार ।
सुनते हैं फिरंगी गारद द्वारा हुक्म की तामील की गई थी।
क्या सोच रही हूँ ! कोई सपना देख रही हूँ।
नहीं, जो सामने हो उसे सौ बरस पुराना किस्सा कैसे मिटा देगा।
हर कदम के साथ यह लगा कि अब जो आँखों के सामने है जो वही हकीकत है। यह भी लड़ाई है। युद्ध है। इसमें हम हारे हैं कि जीते हैं। आजादी। आजादी और विभाजन, दोनों एक साथ।
‘डार से बिछुड़ी’ के इस नए संस्करण में आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है चिल्लियाँवाले मैदान का वह नक्शा जहाँ एक ओर खालसा फौजें थीं और दूसरी ओर फिरंगी की सेनाएँ थीं।
हमारी पराजय का निर्णायक दिन था 21 फरवरी 1849। अंग्रेज और खालसा सेनाओं के वर्णन ऐतिहासिक वृत्तान्त का हिस्सा है।
इस बीच कई बरस बीत गए। टुकड़ों-टुकड़ों में जाने क्या अन्दर जमा होता रहा। इसकी प्रतीति तभी हुई जब ‘डार से बिछुड़ी’ लिखनी शुरू की।
एक रात मेज पर बैठी थी कि कोई चुपके से कान में दोहरा गया। जिएँ-जागें। सब जिएँ-जागें।
उलाहने, शिकायत, दुख-दर्द, कड़ुवाहट भुलाकर कौन कह रहा था कि सब जिएँ-जागें।
यह पोशो की आवाज़ थी। शायद वही लड़की जो उस शाम कर्जन रोड पर चलते-चलते मुझे शाहआलमी में दीखी थी।
न शिक्षा थी न विद्या थी, न पिता की छाँह। न विधवा माँ की मान-मर्यादा और न परिवार की सुरक्षा।
रात के अँधेरों में घर की देहरी से बाहर पाँव रखा और हर कदम दूर होती चली गई पाशो अपनों और परायों से। आकाश में उड़ते पाखियों की डारों से अलग हुए पंछी की तरह।
जिएँ ! जागें ! सब जिएँ-जागें !
अच्छे बुरे, पराए-अपने जो भी मेरे कुछ लगते थे—सब जिएँ !
‘डार से बिछुड़ी’ का सहज सीधा पाठ बिना किसी शिल्प के सहारे स्वयं ही अपने समय सूत्र गूँथता गया और मेरे बाहर के कथ्य को कहानी की आन्तरिकता की ओर मोड़ ले गया। मुझे इस दबाव का अहसास तक न हुआ। इतना ही लगा कि मैं मात्र इसे प्रस्तुत करने के निमित्त हूँ।
‘डार से बिछुड़ी’ का पाठ लिखने में कुछ ऐसा बना कि जैसे पहले ही लिखी जा चुकी इबारत को मन से कागज पर उतारना हो। कोई झिझक, सन्देह या भाषायी उलझन नहीं हुई और फिरंगी की छावनी में पहुँच कहानी अपने आप ही समाप्त हो गई।
लिफाफे पर ‘निकष’—इलाहाबाद का पता लिखा और ‘डार से बिछुड़ी’ को डाक से ‘निकष’ के सम्पादक धर्मवीर भारती को विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया। मन में न छपने की बेचैनी थी और न ही उत्सुकता। नए लेखक वाली कोई चिन्ता और उत्तेजना भी नहीं थी।
‘निकष’ ने जब इसे विशेष कृति करके प्रकाशित किया तो देखकर विस्मय हुआ और न ही विशेष उल्लास की प्रतिक्रिया। ‘डार से बिछुड़ी’ के पाठ से जो उम्मीद उसके लेखक को थी, ‘निकष’ सम्पादक ने उसकी ताईद की थी। इतना कम नहीं था।
‘निकष’ में कहानी को पढ़ा। कहीं कुछ बदला न गया था। कोई परिवर्तन नहीं। सही समय पर मैं आश्वस्त हुई। ‘डार से बिछुड़ी’ के प्रकाशन के साथ ही मेरी रचनाओं पर नजर रखी जाने लगी। लेखक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार और भला क्या हो सकता था ! ‘डार से बिछुड़ी’ के पाठक और सुधी आलोचकों, पाठकों के प्रति गहरे भाव से कृतज्ञ हूँ। हाल ही में जब इसे पढ़ा तो लगा कहानी कहने की यह रफ्तार मुझे अब भी कायम रखनी चाहिए थी। विनम्रतापूर्वक इतना ही कि अपने बलबूते पर मेरे हाथ से उधड़ती चली गई।
विभाजन के बाद के दिन थे। दिल्ली के आकाश पर उतरा हुआ था फरवरी का पत्तों और हवाओं भरा उड़ता-फड़फड़ाता मौसम। अपने जन्म के महीने में मैं हमेशा कुछ अस्थिर सी हो उठती हूँ। धूल-भरी हवाओं सी हरहराती हूँ। बैसाख के उतरने से पहले उखड़-सी जाती हूँ। बहती सरसराती हवाएँ जाने मुझसे क्या कहती हैं। अन्तर की रहस्य-पट्टी से जाने कैसे-कैसे उदास फीके सन्देश भेजती हैं, जैसे कहीं भगदड़ मची हो। दीवारें हिल रही हैं। दरारें दीख रही हों।
फिर वही दिल दहलाता शोर—
अल्लाह ओ अकबर।
हर-हर महादेव।
विभाजन
बँटवारा।
1947।
सुबह-शाम नई दिल्ली की टैंकर से धुलनेवाली तारकोली सड़कों की रंगत बदल गई थी। पटरियाँ उदास, गुस्सील, गमगीन शरणार्थियों को टोलियों से अटी पड़ी थीं। मैली-कुचैली, पगड़ियाँ और दुपट्टे। घायल लुटे नुचे लोगों के ठट्ट के ठट्ट। कैम्प।
बेवतनों के नए नागरिक वार्ड बन रहे हैं।
अपने ठीयों से उखड़े हुए, जड़ों से दूर बदहवास, फिक्रमन्द ख़लकतें और एक दूसरे को रौंदता भाषायी शोर ! खड़े-खड़े लड़ाई-झगड़े। अपनी तल्खियों को उतार फेंकने के लिए तू-तू मैं-मैं, हाथापाई, धक्का-मुक्की। जाने किस-किस शहर के मुर्दा साये बचे-खुचे अपने इलाकेवालों के साथ भटकते छितरते-छिटकते राजधानी में आ जुटे थे।
भीड़ कभी पी ब्लाक, कभी री-हैबिलिटेशन मंत्रालय, कभी पुराना किला, फिरोजशाह कोटला, किंग्सवे कैम्प। कभी रोटी-मजूरी की जुगाड़ में तुर्कमान अजमेरी गेट, काज़ी हौज, खारी बाउली, फतेहपुरी, लाल किला, जामा मस्जिद। चाँदनी चौक।
एक दुपहर मैसोनिक लॉज की डिस्पैंसरी पर लगी लाइनों पर खड़े शरणार्थियों के कार्ड बनवाने की ड्यूटी लगी थी हमारे ग्रुप की। वहीं खड़ी भीड़ में माँ के कंधे से लगे एक बच्चे का भयानक चेहरा देखकर दिल दहल गया। एक आँख और माथे पर लगे दो गहरे घाव। ऊपर भिनभिनाती मक्खियाँ।
विभाजन जब होना ही था तो यह वहशीपन क्यों न रोका जा सका ! नस्लकुशी ?
अपने को घुड़का। बस। इस ओर सिर्फ देखो, उस पर सोचो नहीं।
सिंधिया हाउस का चौराहा क्रास कर कर्जन रोड की पटरी चलने लगी थी। घर लौटते हुए चाल में गहरी बेहिम्मती, थकान। अंग्रेजी हुकूमत का यहाँ से अलग होने का क्या और कोई रास्ता नहीं था !
चलते-चलते आसमान की ओर देखा। लगा एक बहुत बड़ी रस्सी पर ज़ख्मी घायल और मरे हुए लोगों के कपड़े एक साथ सूख रहे हैं। घबराकर अपने को धमकाया। खबरदार। अब इन ख्यालों से अपने को दूर रखो। परे झटक दो और सड़क के साथ-साथ लगे इन छाँहदार हरे भरे पेड़ों की ओर देखो। अपनी हस्ती में मजबूती से जमे हैं और अपनी गहरी जड़ों से। जो उखड़कर सड़कों पर पड़े हैं—उनके लिए जो भी कर सको करो।
पास से गुजरी साइकिल की आवाज़ से चौकी।
यह क्या ?
कर्ज़न रोड की पटरी पर आखों के सामने शाहआलमी प्रकट हो गया। सजी-बनी छोटी-बड़ी दुकानें-चुस्त-चालाक-जवान-बूढ़ी अधेड़ भीड़। माँओं की उँगलियों पकड़े बच्चे। हिन्दुआनियाँ, मुसलमानियाँ, रंग-बिरंगी चुन्नियाँ, चुटले, चूड़ियाँ, सब्जियाँ, फल ललारियों के यहाँ सूखती पगड़ियाँ। एकाएक कोई मुखड़ा झिलमिलाया जैसे भीड़ में से कोई शिलालेख ऊपर आया।
नकोर कंवर का शरमाता, इतराता मुखड़ा। पीले छींट के जोड़े पर हरी-भरी ओढ़नी। चुन्नी के छोर को मुँह में दबाए आँखों से हँसती यह लड़की कहाँ से आ रही है। आँखों से हँसती सयानी होने को मचलती यह बचपनी लड़की। शायद कंजक पुजाने का होगा यही इसका अन्तिम अवसर। फिर बँध जाएगी यह अमावस्या और पूर्णिमा की परिक्रमा से। रजस्वला। मुनिया गुणिया बन जाएगी।
इस लड़की का भला नाम क्या होगा।
पूँछूँ।
भीड़ में अदृश्य हो गई वह लड़की। और मैं चलने लगी सर्राफे की ओर। रुपहली सुनहली जेवर और झक्क मोतियों की जड़त।
मोड़ से बाएँ मुड़ती हूँ।
सोबतियों की हवेली।
हवेली का ऊँचा, चौड़ा पीतल की कीलोंवाला लड़की का पुराना दरवाजा।
फाटक की चौड़ाई और ऊँचाई बाँटते अलग-अलग चार शहतीर। एक-एक के दो-दो टुकड़े। पहले एक को ऊपर उठाओ, फिर दूसरा। इधर का। उधर का। उस पर लटक रहा है ककराली का लोहारी जन्द्रा। इसकी ताली अब किसके पास होगी। जो इधर से वहाँ पहुँचे हैं उनके पास कि उधर वालों के हाथ।
इधर।
उधर।
सामने बड़े सहन के बीच ऊँचे चबूतरे पर पानी की कुँई। लोहे की चरखड़ी। गदर, लड़ाई और भगदड़ों में पानी तो हो पीने वालों के लिए। अन्दर जाते लम्बे बड़े गलियारे पर मुखद्वार। छोटी ईंट की बड़ी ड्यौढ़ी। ड्यौढ़ी के दोनों ओर से ऊपर की मंजिल की ओर जाती सीढ़ियाँ। नीचे किनारे से मुड़ती तहखानों की ओर उतरती सँकरी पैड़ियाँ। मैं जितनी बार वहाँ जाती उतनी बार कई-कई बार नीचे जाती पैड़ियाँ उतरती और दूसरे घुमाव पर रुकती और वापस लौट आती। एक दिन ऊपर से देख रही माँ ने आवाज़ दी—क्या कर रही हो वहाँ। यह खेलने की जगह नहीं।
मैं तहखाने की ओर जा रही थी।
फिर रुक क्यों गई !
डर लगता है। वहाँ साँप है।
तो लौट आओ।
इसे कैसे देख सकती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ। कैसे देखूँ।
ऐसा कोई बन्दा नहीं जो तहखाने में जाए बिना उसे देख सके। इसका ख्याल छोड़ दो।
इसके जवाब के लिए मुझे क्यों रुकना था। जल्दी-जल्दी सीढ़ियाँ उतर गई और तहखाने का पल्ला धकियाया और किवाड़ का आधा पाट चरमराया। और इस आधे का टुकड़ा खिसियाना सा खुला। तहखाने की बासी-मुसी सीलन-भरी दुर्गन्ध नाक में घुस गई। पहले अपने कपड़ों को झाड़ा। आँखें गड़ाईं। अन्दर अँधेरा है। वहाँ से उभरी छोटी सी लीक रोशनी की। सामने की दीवार पर झरोखी है। देख लूँगी। कुछ को देख सकूँगी। कुछ-कुछ दिखता है। वह क्या ? टँगने पर लटक रहे हैं, लिहाफ़। चिमगादड़। और यह क्या ? दो बटनों की-सी आँखोंवाला उल्लू। उल्लू ही है। चुपचाप बैठा है। चिमगादड़ तो फड़फड़ाता है। बालों में फँस जाता है। यह बड़े-बड़े मटके। इनमें सिक्के होंगे।
सिक्के और तलवारें—लड़ाई के वक्त छावनी और शहर में अंग्रेजों का पहरा लग गया था। तहखानों और सिक्ख-फिरंगी युद्ध की जाने कितनी कहानियाँ हमने सुन रखी थीं।
गुजरात के चिल्लियाँवाले मैदान में तीसरी लड़ाई में अंग्रेजों ने हमें हराकर पंजाब को जीता था।
अपनी सेनाओं को पराजित कर अंग्रेजों ने शहर-भर में अपनी विजय का ऐलान कर दिया था। गलियों, नाकों और हवेलियों के मुख्य द्वारों पर फिरंगी गारद के पहले लग गए। रात के पहले पहर हमारे परिवार की सयानी पुरखन तहखानों में उतरी। अँधेरे में हरिसिंगे सिक्के झोली में डाले और पैड़ियों से ऊपर चढ़ी। जाने किस हड़बड़ाहट में सिक्के नीचे गिर पड़े और ड्योढ़ी के सामने बिखर गए। गारद ने मुड़कर देखा तो सयानी पुरखन ने रोबीली आवाज़ में हुक्म दिया—उठाओ और इधर लाओ। मुझे दो।
आवाज़ थी कड़ाकेदार ।
सुनते हैं फिरंगी गारद द्वारा हुक्म की तामील की गई थी।
क्या सोच रही हूँ ! कोई सपना देख रही हूँ।
नहीं, जो सामने हो उसे सौ बरस पुराना किस्सा कैसे मिटा देगा।
हर कदम के साथ यह लगा कि अब जो आँखों के सामने है जो वही हकीकत है। यह भी लड़ाई है। युद्ध है। इसमें हम हारे हैं कि जीते हैं। आजादी। आजादी और विभाजन, दोनों एक साथ।
‘डार से बिछुड़ी’ के इस नए संस्करण में आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है चिल्लियाँवाले मैदान का वह नक्शा जहाँ एक ओर खालसा फौजें थीं और दूसरी ओर फिरंगी की सेनाएँ थीं।
हमारी पराजय का निर्णायक दिन था 21 फरवरी 1849। अंग्रेज और खालसा सेनाओं के वर्णन ऐतिहासिक वृत्तान्त का हिस्सा है।
इस बीच कई बरस बीत गए। टुकड़ों-टुकड़ों में जाने क्या अन्दर जमा होता रहा। इसकी प्रतीति तभी हुई जब ‘डार से बिछुड़ी’ लिखनी शुरू की।
एक रात मेज पर बैठी थी कि कोई चुपके से कान में दोहरा गया। जिएँ-जागें। सब जिएँ-जागें।
उलाहने, शिकायत, दुख-दर्द, कड़ुवाहट भुलाकर कौन कह रहा था कि सब जिएँ-जागें।
यह पोशो की आवाज़ थी। शायद वही लड़की जो उस शाम कर्जन रोड पर चलते-चलते मुझे शाहआलमी में दीखी थी।
न शिक्षा थी न विद्या थी, न पिता की छाँह। न विधवा माँ की मान-मर्यादा और न परिवार की सुरक्षा।
रात के अँधेरों में घर की देहरी से बाहर पाँव रखा और हर कदम दूर होती चली गई पाशो अपनों और परायों से। आकाश में उड़ते पाखियों की डारों से अलग हुए पंछी की तरह।
28 जुलाई 2001
-कृष्णा सोबती
एक
जिएँ ! जागें ! सब जिएँ जागें !
अच्छे, बुरे, अपने, पराए—जो भी मेरे कुछ लगते थे सब जिएँ !
घड़ी भर पहले चाहती थी कि कहूँ सब मर-खप जाएँ। न कोई जिए न जागे। मैं मरूँ तो सबको ले मरूँ ! इस अभागी के ही जीने के लेख बिसर गए तो कोई और क्यों जिए ? क्यों जागे ?
पर कौन होती थी मैं अपने दुर्भाग्य से हरी-भरी बेलों को जला देनेवाली ! कौन होती थी मैं दूध-भरी झोलियों को सुखा देनेवाली ! कौन होती थी मैं भरी-भराई, लाड-सनी झोलियों को दहला देनेवाली !
मालिक के किए जब भरी रही मेरी झोली, हरी रही मेरी झोली, तो क्यों न लोक-जहान फले-फूले ! क्यों न अपने-पराये जिएँ-जागें ! हँस-खेलें उनकी भरी पूरी गृहस्थियाँ, जिन्होंने बाँहें बढ़ा मुझ कर्मजली को अपनी डार से मिला लिया।
सब जिएँ ! सब जागें !
पर जो मैं थी, वह क्या फिर से लौट आई हूँ ?
भरे उठान अकड़कर, आँखों से रंगीन डोरे बिखेरते राह पर से चली जाती ! ठहरने को न कपड़ा ठहरता, न नजर ! और बाँहें प्यासी गलबहियों-सी हर अँगड़ाई के संग उठती, खिलतीं और अपने में सिमट जातीं !
शाह आलमी से जब तिल्लेवाली नोकदार जूती पहने, फुम्मनियोंवाला लम्बा पराँदा डुलाते निकलती तो आवाज़ें सुन-सुन मुस्कुराती !
माँ क्या मुझसे कम रही होंगी ! खोजों के घर पटरानी बनकर बैठ जानेवाली नानी की बेटी कैसी लगती होगी ? बार-बार सोचती और सोच-सोचकर और भी इठलाती। चाहती, किसी दिन चुपके से खोजों की हवेली जाऊँ और किसी झरोखे से अपनी माँ कहलाने वाली की एक झलक पाऊँ। पर अपने छोटे-बड़े मामू के कठोर चेहरे याद कर पाँव ठिठक जाते। बहाने-बहाने शाह आलमी तक निकल जाती और कुम्हारों के घर तक हो वापस लौट आती।
कभी नानी के संग ठाकुरद्वारे जाती तो नानी तेवर सिर चढ़ा सिर ठोकती—
‘‘रब्ब तुझे सँभाले, अरी कपड़ा नीचे रखा कर !’’
कुएँ से गागर भरकर लाती तो बड़ी माँमी आँखें तरेरती; फिर क्रोध से बाँह में अटकी गागर खींचकर कहती—
‘‘पसार छूने लगी—न शर्म, न हया ! अरी, ओढ़नी अब तेरे गले तक से उठने लगी...।’’
मैं गोल-गोल आँखों से सामना किए रहती, न पलक झपकती, न कुछ कहती। बस छिपी-छिपी नजर अपने चाँदी के बीड़ेवाले कुरते को निहारती।
तन्दूर तपा परात में से आटा ले-ले पेड़े बनाती थी कि छोटे मामू सीढ़ियाँ चढ़े; चूड़ियों की खनकार सुन जैसे ठिठक गए।
पानी से छुआ, झुक तन्दूर में हाथ डाला सेंक न सहार सकने से उछलकर पीछे हुई कि छोटे मामू ने निर्दयता से चुटिया घुमा दी और धक्का देकर कहा—
‘‘अरी, यह कुलच्छनियोंवाले हाव-भाव !’’
आवाज सुन नानी बाहर निकल आई। घड़ी-भर सहमी-सी मामू की ओर देखती रही, फिर हाथ से तिरस्कारती बोली—
‘‘अरी कुएँ में डूब मरी थी तेरा बीज डालनेवाली ! अब तू सँभलकर साँस भर....!
एक बार तो आँसू छलके, फिर ओढ़नी मुँह में डाल रोती रही ! खड़ी रही—खड़ी रही। फिर जलती रोटी तन्दूर से निकाल चँगेर में डाली और दूसरा पूर लगाने लगी।
नानी कान की बड़ी-बड़ी मुरकियाँ हिला-हिला बोली—
‘‘जा बेटा, कुछ पानी-धानी पी...’’
मामू जाते-जाते फिर रुके और बाँह फैलाकर बोले—
‘‘तन्दूर लगाने को क्या यही चुड़ैल रह गई है ? इसे बर्तन-भाँड़े दिया करो मलने को...’’
अच्छे, बुरे, अपने, पराए—जो भी मेरे कुछ लगते थे सब जिएँ !
घड़ी भर पहले चाहती थी कि कहूँ सब मर-खप जाएँ। न कोई जिए न जागे। मैं मरूँ तो सबको ले मरूँ ! इस अभागी के ही जीने के लेख बिसर गए तो कोई और क्यों जिए ? क्यों जागे ?
पर कौन होती थी मैं अपने दुर्भाग्य से हरी-भरी बेलों को जला देनेवाली ! कौन होती थी मैं दूध-भरी झोलियों को सुखा देनेवाली ! कौन होती थी मैं भरी-भराई, लाड-सनी झोलियों को दहला देनेवाली !
मालिक के किए जब भरी रही मेरी झोली, हरी रही मेरी झोली, तो क्यों न लोक-जहान फले-फूले ! क्यों न अपने-पराये जिएँ-जागें ! हँस-खेलें उनकी भरी पूरी गृहस्थियाँ, जिन्होंने बाँहें बढ़ा मुझ कर्मजली को अपनी डार से मिला लिया।
सब जिएँ ! सब जागें !
पर जो मैं थी, वह क्या फिर से लौट आई हूँ ?
भरे उठान अकड़कर, आँखों से रंगीन डोरे बिखेरते राह पर से चली जाती ! ठहरने को न कपड़ा ठहरता, न नजर ! और बाँहें प्यासी गलबहियों-सी हर अँगड़ाई के संग उठती, खिलतीं और अपने में सिमट जातीं !
शाह आलमी से जब तिल्लेवाली नोकदार जूती पहने, फुम्मनियोंवाला लम्बा पराँदा डुलाते निकलती तो आवाज़ें सुन-सुन मुस्कुराती !
माँ क्या मुझसे कम रही होंगी ! खोजों के घर पटरानी बनकर बैठ जानेवाली नानी की बेटी कैसी लगती होगी ? बार-बार सोचती और सोच-सोचकर और भी इठलाती। चाहती, किसी दिन चुपके से खोजों की हवेली जाऊँ और किसी झरोखे से अपनी माँ कहलाने वाली की एक झलक पाऊँ। पर अपने छोटे-बड़े मामू के कठोर चेहरे याद कर पाँव ठिठक जाते। बहाने-बहाने शाह आलमी तक निकल जाती और कुम्हारों के घर तक हो वापस लौट आती।
कभी नानी के संग ठाकुरद्वारे जाती तो नानी तेवर सिर चढ़ा सिर ठोकती—
‘‘रब्ब तुझे सँभाले, अरी कपड़ा नीचे रखा कर !’’
कुएँ से गागर भरकर लाती तो बड़ी माँमी आँखें तरेरती; फिर क्रोध से बाँह में अटकी गागर खींचकर कहती—
‘‘पसार छूने लगी—न शर्म, न हया ! अरी, ओढ़नी अब तेरे गले तक से उठने लगी...।’’
मैं गोल-गोल आँखों से सामना किए रहती, न पलक झपकती, न कुछ कहती। बस छिपी-छिपी नजर अपने चाँदी के बीड़ेवाले कुरते को निहारती।
तन्दूर तपा परात में से आटा ले-ले पेड़े बनाती थी कि छोटे मामू सीढ़ियाँ चढ़े; चूड़ियों की खनकार सुन जैसे ठिठक गए।
पानी से छुआ, झुक तन्दूर में हाथ डाला सेंक न सहार सकने से उछलकर पीछे हुई कि छोटे मामू ने निर्दयता से चुटिया घुमा दी और धक्का देकर कहा—
‘‘अरी, यह कुलच्छनियोंवाले हाव-भाव !’’
आवाज सुन नानी बाहर निकल आई। घड़ी-भर सहमी-सी मामू की ओर देखती रही, फिर हाथ से तिरस्कारती बोली—
‘‘अरी कुएँ में डूब मरी थी तेरा बीज डालनेवाली ! अब तू सँभलकर साँस भर....!
एक बार तो आँसू छलके, फिर ओढ़नी मुँह में डाल रोती रही ! खड़ी रही—खड़ी रही। फिर जलती रोटी तन्दूर से निकाल चँगेर में डाली और दूसरा पूर लगाने लगी।
नानी कान की बड़ी-बड़ी मुरकियाँ हिला-हिला बोली—
‘‘जा बेटा, कुछ पानी-धानी पी...’’
मामू जाते-जाते फिर रुके और बाँह फैलाकर बोले—
‘‘तन्दूर लगाने को क्या यही चुड़ैल रह गई है ? इसे बर्तन-भाँड़े दिया करो मलने को...’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book